पद्मावती समय
Padmavati Samaya
भाग – 6 (भावपक्ष-कलापक्ष)
भाव पक्ष
' पद्मावती समय ' चन्दबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण अंश है । यद्यपि पृथ्वीराज रासो को कुछ विद्वानों ने ऐतिहासिक वीर गाथात्मक काव्य माना है , लेकिन इसमें कल्पना तत्त्व का इतना अधिक समावेश हो गया है कि उसका इतिहास पक्ष पूर्णतः दब गया है । वस्तु - वर्णन की दृष्टि से पृथ्वीराज रासो और पद्मावती समय एक उल्लेखनीय रचना मानी जाती हैं काव्य - शास्त्र की दृष्टि से वस्तु - वर्णन को महाकाव्य का एक गुण माना गया है । समूचा रासो काव्य वर्णनों का भण्डार है । अतः पद्मावती समय कोई अपवाद नहीं है । इसमें भी हमें वस्तु - वर्णन के अनेक स्थल देखने को मिल जाते हैं । भले ही ' पद्मावती समय ' पथ्वीराज रासो का ही एक अंश है , लेकिन इसे स्वतंत्र खण्ड काव्य कहना अधिक उचित होगा । पद्मावती समय के वस्तु वर्णन को निम्न प्रकार विवेचित किया जा सकता है
वस्तु वर्णन
जहां तक वस्तु वर्णन का प्रश्न इस काव्य रचना के पांचवें छन्द में ही वह शुरु हो जाता है । पद्मावती ने ही सर्वप्रथम शुक से उसका परिचय पूछा । उत्तर के रूप में शुक पृथ्वीराज का वर्णन करता हुआ कहने लगा कि हिन्दुस्तान में दिल्ली गढ़ नामक एक नगर है । वहां इन्द्र का अवतार चौहान वंशी , अत्यन्त वीर और बलवान राजा पृथ्वीराज है । ' तह पथिराज सुर सुभार ' दिल्ली नगरी के राजा के वंश की गौरव - गाथा का वर्णन करता हुआ वह कहता है
- ' संघरि नरेस पहुआन पानं , पथिराज तई बाजंत भान ।
- बैसह बरीस बोडस नरिवं , पूत , आजानु बाहु मुअजोक बंद ।।
- संगरि नरेस सोमेस पूत , देवंत रूप अवतार दूत ।
- तासु मंसूर सबै अपार भूजानं भीम जिम सार भार ।।
शुक पद्मावती को यह भी बताता है कि पृथ्वीराज इतना शक्तिशाली राजा है कि उसने शहाबुद्दीन गौरी को तीन बार पकड़ लिया था और उसकी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दिया था । यही नहीं वे अचूक शब्द भेदी बाण को चलाने का भी सामर्थ्य रखते हैं ।
सैन्य – वर्णन
' पद्मावती समय ' में कवि ने जो सेना का वर्णन किया है वह वीर भाव को उद्दीप्त करने वाला है । इसमें कवि की वीर रस प्रवणता देखने को मिलती है । एक स्थल पर कवि ने शहाबुद्दीन गौरी की सेना का जो वर्णन किया है , वह बड़ा ही आकर्षक बन पड़ा है । कवि लिखता है कि
- " क्रोध जोध जोधा अनंत किरिय पन्ती अनि - राज्जिय ।
- बान नालि बनालि तुपक तीरह , सब रज्जिय ।।
- पर्व पहार मनो सार्क के , भिरि भुजान गपनेस बल ।
- आए हकारि हकारि भुरिपुरासान सुलतान दल ।। "
इन पंक्तियों में क्रोधित योद्धाओं के समूह , चिंघाड़ते हुए हाथियों , धनुष बाण , तोप आदि से सुसज्जित सेना का यथार्थ वर्णन किया गया है । कवि ने अनेक स्थलों पर सैन्य सज्जा और योद्धाओं की मनोवृत्तियों का उल्लेख किया है । कवि यह भी स्पष्ट करता है कि शहाबुद्दीन की सेना में खुरासानी , कंधारी , तुर्की , फिरंगी आदि सैनिक थे । इन सब की रूप - रचना अलग - अलग प्रकार की थी । यही नहीं , कवि ने सेना के अश्वों का भी बड़ा ही प्रभावशाली वर्णन किया है । सेना के घोड़ों में ताजी , तुर्की , महावाणी , कमानी तथा वाजि आदि अनेक नस्लों के घोड़े थे । यथा
- " जहां बाग बाछ मसरी रिछोरी ।
- धर्म सार समूह अरू चौर मारी ।
- एराकी , अदब्बी , पटी , तेज , ताजी ।
- तुरक्की , महावन , कम्मान बाजी ।। "
युद्ध वर्णन
पृथ्वीराज रासो युद्ध - वर्णन के लिए हिन्दी साहित्य में एक उल्लेखनीय रचना मानी जाती है । क्योंकि पद्मावती समय रासो का ही एक खण्ड है , अतः इसमें भी शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज चौहान के युद्ध का सजीव वर्णन मिलता है । कुछ पद्यों में युद्ध की क्रियाओं का वर्णन इतना सूक्ष्म है कि पाठक उन्हें पढ़ते ही भाव - विभोर हो जाता है । युद्ध वर्णन करते समय कवि भयानक और वीभत्स दृश्यों का चित्र अंकित कर देता है । एक उदाहरण दर्शनिय है
- " न को हार मह जित्त , रहेज न रहहि सुखर ।
- घर उप्पर भर परत करत अति जुद्ध महाभर ।
- कहाँ कम कहाँ मध्य कहाँ कर घर व अंतरूरि ।
- कहाँ कंच बहि तेग , कहाँ सिंर पुटि उर ।।
- कहाँ देत मेत हम पुर पुपरि , कुंभ मसुंबह कंड सव ।
- हिंदवान शंनभय मांन मुष गहइ तेग चहुआन जबु ।।
उपर्युक्त उदाहरण में कवि ने अन्तिम चार पंक्तियों में जुगुप्सा जनक चित्र अंकित किया है । यहां भयंकर युद्ध का वर्णन है जिसमें असंख्य योद्धा मर - कट रहे हैं । कहीं तो योद्धाओं के कबन्ध पड़े है तो कहीं सिर पड़े हैं । हाथ - पांव कटकर अलग बिखरे पड़े हैं । किसी की अंतड़ियां पेट से बाहर निकल आई है तो किसी का कंधा अलग हो गया है । उधर पृथ्वीराज के सैनिक शत्रुओं की सेना पर ऐसे टूट रहे हैं जैसे शेर हाथियों पर टूटते हैं । स्वयं पृथ्वीराज एक सिंह के समान शत्रुओं पर आक्रमण कर देते हैं । जिसके फलस्वरूप शत्रु सेना में भगदड़ मच जाती है । सूंड कट जाने के कारण हाथी चिंघाड़ मारकर भाग रहे हैं जिसके फलस्वरूप युद्ध भूमि में खलबली मच गई है । उदाहरण दर्शनीय है
- " करीचीह चिक्कार करि कलप भग्गे ।।
- मंद तंथि लाज ऊमग मग्गे ।।
- दोरि गज अंध चहुआन केरो ।
- घेरियं गिरछ विहाँ चक्क फेरो ।। "
सौन्दर्य - चित्रण
' पद्मावती समय नख - शिख वर्णन के लिए भी एक उल्लेखनीय काव्य रचना है । समुदशिखर की राजकुमारी पद्मावती इस काव्य की नायिका है । वह अनिंद्य सुन्दरी होने के साथ - साथ एकनिष्ठ प्रेमिका भी है । अभी तक उसने वयःसन्धि को ही प्राप्त किया है । लेकिन फिर भी वह सम्पूर्ण कलाओं , चौदह विधाओं तथा वेद - शास्त्र आदि में पूर्णतया प्रवीण है । उसमें नायिका के सभी गुण और सामुद्रिक लक्षण विद्यमान हैं । कवि ने उसके सौन्दर्य का वर्णन करते हुए लिखा है
- " मनहुं कला ससि भान , कला सोलह सो बनिय ।
- बाल बेस ससि ता समीप , अम त रस पिन्निय ।।
- बिगसि कमल निग अमर , बैन.पंजन मग लुट्टिय ।
- हीर कीर अरू विम्म मोति नष सिप अहि पुट्टिय ।।
- छप्पति गयन्द हरि हंस गति , विह बनाय संचे सचिय ।
- पदमिनिय रूप पद्मावतिय , मनहुं काम कामिनि रषिय ।।
" उपर्युक्त पद्य से स्पष्ट होता है कि यहां कवि ने पद्मिनी नायिका के सभी लक्षण पद्मावती में घटाए हैं । तोता भी उसके अद्वितीय सौन्दर्य को देखकर उसे पद्मिनी नायिका ही मानता है । लेकिन कवि ने तो सामुद्रिक शास्त्र के सभी लक्षण उसे नायिका घटा दिए हैं । नायिका पद्मगंधा नायिका है , क्योंकि उसके शरीर से कमलों की सुगंध उठती है इसलिए कवि लिखता है
" कमलगंध , वयसंध , हंसगति चलत मंद - मंद भमर भवहि भुल्लाह सुभाय मकरन्द बास रस ।। "
पद्मावती के रूप - सौन्दर्य के वर्णन को पढ़कर कभी कभी पाठक को जायसी के पद्मावत की याद आ जाती है । वहां पर भी हीरामन तोते द्वारा पद्मावती का नख शिख वर्णन राजा रत्नसेन के समक्ष किया जाता हैं इस काव्य - रचना में भी तोता पद्मावती का रूप वर्णन महाराज पृथ्वीराज के समक्ष जाकर करता है । उसके नख - शिख वर्णन को सुनकर ही पृथ्वीराज चौहान पद्मावती को प्राप्त करने के लिए समुदशिखर पर आक्रमण कर देता है । एक स्थल पर ही कवि ने पद्मावती को मुग्धा नायिका के रूप में चित्रित किया है । लेकिन आगे चलकर पद्मावती एक विरहिणी नायिका के रूप में भी वर्णित की गई है ।
प्रकृति चित्रण
प्रकृति का स्वच्छन्द विस्तृत गंभीर वर्णन पथ्वीराज रासो में उपलब्ध नहीं होता । लेकिन जितना भी उपलब्ध होता है वह अत्यन्त सजीव और स्वाभाविक है । पृथ्वीराज रासो में ऋतुओं के वर्णन के अन्तर्गत प्रकति का वर्णन किया गया है । इस संबंध में कवि ने ग्रीष्म ऋतु , शिशिर ऋतु शरद् ऋतु , हेमन्त तथा बसन्त आदि ऋतुओं का हृदयग्राही वर्णन किया है । पृथ्वीराज रासो से ही एक उदाहरण जिसमें शिशिर ऋतु के बारे में वर्णन किया गया है
- " रोमालत धन नीर निब्ध परये गिरि ढंग नारायते ।
- पव्यय पीन कुचानि पानि समला पुंकार मुकारये ।।
- शिशिरे सबरि बारुणे च विरहा मम ब्रदय विदारये ।
- मां कार्मत मृग बद्ध सिंध मने किं देव उबारये ।।
" इसी प्रकार से कवि ने कुछ स्थलों पर प्रकति का आलम्बन रूप में भी वर्णन किया है । ऐसे वर्णन पाठक को सहज प्राकृतिक सौन्दर्य की अनुभूति कराने में सक्षम हैं ।
बारात - वर्णन
' पद्मावती समय ' में बारात का भी रमणीय और आकर्षक वर्णन कवि ने किया है । इस वर्णन से कवि ने बारात के सभी पक्षों पर प्रकाश डाला है । कहीं तो कवि विशाल हाथियों और उनके गंडस्थलों से टपकने वाले मदस्राव का वर्णन करता है तो कहीं उनके श्वेत दांतों का । इस वर्णन में कवि ने संश्लिष्ट बिम्बों की रचना की है । बारात का वर्णन करते समय कवि ने वाद्य यन्त्रों तथा उनसे उत्पन्न होने वाले संगीत की भी चर्चा की है । इस अवसर पर कवि यह भी नहीं भूला कि बारातियों में विवाह - अवसर के अनुकूल उत्साह और प्रसन्नता दिखाई देती है । यह सारा वर्णन इतना मनोहारी है कि उसे पढ़कर पाठक स्वयं को बाराती समझने लगता है ।
- " चले दस महस्सं असवार जान ।
- पूरियं पैदलं तैतीस बान ।
- मत्त मद गलित से पंच दती ।
- मनो सांम पाहार युगपंत पंती ।।
- चले अग्नि तेज , जुतते तुषारं ।
- चौपट चौरासी जु साकत्ति भारं ।।
यहाँ चन्दबरदाई ने बारात में बजाए जा रहे विभिन्न प्रकार के वाद्य यन्त्रों का भी वर्णन किया है जिनमें नाल , तंनी , नगाड़ा , झांझ और तुरही आदि एक साथ बजाए जा रहे थे । ' पद्मावती समय ' मूलतः लघुकाव्य है । इसे खण्ड काव्य भी कहा जा सकता । अतः- इसमें वर्णन लिए अधिक स्थान नहीं है । जहां पृथ्वीराज रासो में प्रकति वर्णन तथा समाज का वर्णन प्रभूत मात्रा में मिल जाता है , वहां इसमें अल्प मात्रा में है या नहीं है । कवि ने राजाओं के वैभव और शक्ति का खुलकर वर्णन किया है । इसके साथ - साथ कवि ने सेना - वर्णन , युद्ध - वर्णन , नायिका का नख - शिख एवं सौन्दर्य वर्णन काफी सुन्दर किया है । पृथ्वीराज का वर्णन करते समय कवि ने उसके प्रसिद्ध वंश , उदात्त गुणों , वीरता एवं शौर्य का हृदयाकर्षक वर्णन किया है । शाहाबुद्दीन के सेना के साथ हुआ युद्ध - वर्णन काफी विस्तार पा गया है , लेकिन यह वर्णन काफी प्रभावशाली है । इसीलिए कुछ आलोचकों ने वर्णनों की दृष्टि से इस काव्य रचना को कोई विशेष महत्व प्रदान नहीं किया । भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से रचना अत्यन्त प्रभावी है ।
कलापक्ष (काव्य सौन्दर्य)
पद्मावती समय ' चन्दबरदाई कृत महाकाव्य पृथ्वीराज रासो का बीसवां समय ( अध्याय ) के रूप में व्यवस्थित है । पृथ्वीराज रासो में ऐतिहासिकता के साथ - साथ कल्पना का भी सुन्दर मिश्रण किया गया है । कवि ने अपने समय की असंख्य लोक प्रचलित निजंधरी कथाओं का समावेश करके रासो को एक वृहद् आकार प्रदान किया है । पदमावती समय ' इसी प्रकार की एक काव्यात्मक रचना है । इसमें कवि ने अपने अद्भुत काव्य कौशल का परिचय दिया है । वस्तु वर्णन , भावाभिव्यंजना , अलंकार योजना , भाषा , छन्द आदि सभी दृष्टियों से पृथ्वीराज रासो एक महान् काव्य है । पद्मावती समय भी उसी का एक अध्याय है । अतः उसमें हमें कवि की प्रतिभा का वही रूप प्राप्त होता है जो रासो में है । जिसका अध्ययन हम निम्न बिंदुओ से कर सकते हैं –
कथा - संदर्भ
' पद्मावती समय ' अपने वस्तु वर्णन के लिए प्रसिद्ध है । इसमें जहां एक ओर ' पद्मावती के रूप सौन्दर्य , बारात , सेना तथा युद्ध का वर्णन मिलता है वहां दूसरी ओर पद्मावती का नख - शिख वर्णन भी काफी आकर्षक बन पड़ा है । पद्मावती का सौन्दर्य वर्णन करते समय कवि ने सांकेतिक और आलंकारिक भाषा का प्रयोग किया है
" मनहुं कला ससि भान कसा सोलह सों बन्निय ।
बाल वैस ससि ता समीप अमित रस पिन्निय ।
विगसि कमल , भिमर , अनु , खंजन , मग , लुदि ।
महाकवि ने सेना का जो वर्णन किया है वह वीर भव को उत्पन्न करने वाला है । शाहहाबुद्दीन गौरी की सेना का निम्नलिखित वर्णन देखिए
- " क्रोध जोध जोधा अनंत करिय पन्ती अनि - गज्जिय ।
- बानं नालि हथनालि . तुपक , तीरह , सब , रजिय ।।
- पचपहार मनौ साल के . मिरि , मुजान गजनेस बल ।
- आए हकारि हकारि भुरि , परासान सुलतान दल ।। "
युद्ध - वर्णन की दृष्टि से पद्मावती समय ' महाकवि का एक उल्लेखनीय खण्ड काव्य है । इसमें पृथ्वीराज और कुमोद्मणि तथा पृथ्वीराज और शाहाबुद्दीन गोरी के युद्धों का सजीव वर्णन मिलता है । कुछ पदों में युद्ध की क्रियाओं का वर्णन इतना सूक्ष्म है कि पाठक उसे पढ़कर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता । युद्ध वर्णन करते समय कवि भयानक एवं वीभत्स दृश्यों के चित्र अंकित करता है । उदाहरण अवलोकनीय है
- जिय घोर निसांन , रांन पहुंबान यहाँ विसि ।
- सकल सूर सामन्त , समरि बल जंत्र मंत्र तिसि ।।
- उठि राज प्रथिराज , बाग मनों लग वीर नट ।
- पढ़त तेग मन बेग , लगत मनों बीजु भट्ट पट ।।
- थकि रहे सूप कौतिग गिगन , रंगन मगन मनोन धर ।
- हर हरषि वीर जग्गे हुलस , हुख रंगि नव स्त बर ।। "
बारात चित्रण कुमायूं का राजा अपनी बारात लेकर समुद्र शिखर की ओर चल पडता है । बारात में राजकुल के सर्वथा उपयुक्त सेना , हाथी और घोडे हैं । उसकी सेना के दस हजार घुड़सवार , हाथी तथा असंख्य पैदल सैनिक बारात के साथ चल रहे थे । हाथियों के गंड स्थलों से मदस्राव हो रहा था । उनके काले - काले शरीरों से बाहर निकले हुए दांत ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो पर्वतों पर श्वेत बगुलियों की पंक्तियाँ हो , बारात में बजते वाद्य मानो हिरणों को भी सम्मोहित कर रहे थे । निम्नलिखित उदाहरण देखिए
- " चले बस सहससं असबार जान ।
- परियं पैदलं तेतीसु थान ।
- मत मद गलित सी परंच दन्ती ।
- मनो साम पाहार बुगपांति पंती ।।
- चले अम्गि तेजी जु साकति यारं ।
- चौवरं चौरासी जु , साकति यार ।
- कंठ नगं नुपं अनोपं सुलालं ।
- रंग पंच रंग बलकत्त ढालं ।। "
रस
रस की दृष्टि से पद्मावती समय में केवल दो रस ही प्रधान रूप में दिखाई देते हैं । ये हैं – श्रृंगार और वीर – रस । श्रृंगार के दोनों पक्ष संयोग और वियोग देखे जा सकते हैं । युद्ध - वर्णन में वीर , रौद , भयानक तथा वीभत्स रसों की स्थिति मिल जाती है । फिर भी ' पद्मावती समय में वीर - रस ही अंगी - रस है । वैसे पद्मावती समय का आरम्भ भी श्रृंगार रस से होता हैं और अन्त भी श्रृंगार रस से होता है ।
श्रृंगार - रस
यद्यपि इस काव्य रचना में श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनो पक्षों का वर्णन मिलता है लेकिन संयोग श्रृंगार ही प्रधान रूप में वर्णित है । काव्यारम्भ में कवि पद्मावती के अनिंद्य सौन्दर्य का वर्णन आता है । आगे चलकर शुक राजा पृथ्वीराज के समक्ष पद्मावती का रूप वर्णन करता है । वह उसे नायक पृथ्वीराज के सर्वथा योग्य नायिका सिद्ध करता है
- " कुहिल केश सुदेश , पौहप रचियत गिक्क सद ।
- कमल गन्ध वयसंध , हंस - गति चलत मंद मंद ।।
- सेत वस्त्र सोह सरीर , नए सांति बुन्द जस ।
- भमर अंयहि भुलहिं सुभाय , मकरन्द वास रस ।।
- नैन निरखि सुप पाय सुक , यह सुविन मूरति रषिय ।
- उमा प्रसाद हर हेरियत , मिलहि राज प्रधिराज जिय ।। "
अभी तक पद्मावती का प्रेम एकपक्षीय है । दो - तीन पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है कि वह नायक पृथ्वीराज की विरह से व्याकुल । ' तन चिकर चीर डाग्यौ उतारि पंक्ति से भी स्पष्ट होता है कि पद्मावती प्रियतम में की विरह में व्याकुल एवं उदास रहती है । अतः हम कह सकते हैं कि ' पद्मावती समय में वियोग श्रृंगार के लिए अधिक स्थान नहीं है ।
वीर - रस
पृथ्वीराज रासो तथा उसके खण्ड 'पदमावती समय ' को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि चन्दबरदाई वीर रस का वर्णन करने में सिद्धहस्त थे । उन्होंने आरम्भ से ही पृथ्वीराज साहस , वीरता , कौशल आदि का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है । इसी प्रकार कवि ने शहाबुद्दीन गौरी की विशाल सेना का वर्णन भी प्रभावशाली ढंग से किया है । दोनों के युद्ध वर्णन करते समय योद्धाओं की मनःस्थिति पर भी प्रकाश डाला है । पद्मावती समय में कवि ने पृथ्वीराज , विजय , शहाबुद्दीन गौरी और कुमोदमणि जैसे चार राजाओं का वर्णन किया है । पहले तीन राजाओं ( पृथ्वीराज , शाहाबुद्दीन , कुमोदमणि ) के अन्य गुणों के साथ उनकी विशाल सेना का भी वर्णन है . लेकिन शाहाबुद्दीन की तो केवल विशाल सेना का ही वर्णन है । युद्ध से पूर्व कवि रणसज्जा का वर्ण करता है । बाद में भयंकर युद्ध आरम्भ हो जाता हैं और युद्ध क्षेत्र मैं बाणों की वर्षा होने लगती है तथा खून की नदियां बहने लगती है । युद्ध वर्णन करता हुआ कवि लिखता है ।
- " कग्मानं बांन छुट्टिहि अपार ।
- लागत लोह मि सारधार ।
- घमसान घान सबबीर घेत ।
- घन प्रोन बत अरू रकत रेत ।।
युद्ध भयंकर रूप धारण करता है , त्यों - त्यों वीर - रस का वातावरण तैयार होता जाता है । कभी - कभी तो लगता है मानो वीर - रस आकार धारण करके स्वयं युद्ध , क्षेत्र में उतर आया है । एक उदाहरण देखिए
- " न को हार नह जित्त , रहेइन रहिब सूखर ।
- पर उपर भए परत , करत अति जुद्ध महाभर ।।
- कहाँ कम कहाँ मथ , कहाँ कर चरन अन्तरूरि ।
- कहाँ कन्ध बहि वेग , कहाँ सिर जुहि फुट्टि सर ।।
- कहीं दन्त मत्त हय पुर पुपरि , कुम्भ भसुण्डा खण्ड सब ।
- हिन्दबान रानं भय भानं मुष . गहिए तेग चहुंबांन जब ।। "
छन्द-अलंकार
' पद्मावती समय ' में कवि ने अलंकारों का सुन्दर एवं स्वाभाविक प्रयोग किया है , परन्तु इसे सायास नहीं कहा जा सकता । वीर और श्रृंगार दोनों रसों के प्रयोग में कवि ने अलंकारों का सुन्दर प्रयोग किया है । अनुप्रास , उपमा , रूपक , उत्प्रेक्षा , अतिशयोक्ति , यमक , प्रान्तिमान तथा दष्टान्त जैसे अलंकार ' पदमावती समय ' में मिल जाते हैं । पद्य पंक्तियों को पढ़ते समय पाठक को ऐसा लगता ही नहीं कि कोई अलंकार उसके सामने आया है । उदाहरण
उपमा- " रति बसन्त परमानं । नम सांति बुंद जस ।। "
रूपक - मंडल मयंक बर नारि सब ।। "
अनुप्रास- " इसम हयगह देस अति । घर भर रज रवह ।। "
अतिशयोक्ति- " इक नायक कर घरी । पिनाक पर भर रज यह ।। "
कवि चंद को छन्दों का राजा कहा जाता है । एक आलोचक ने तो पृथ्वीराज रासो को ' छन्दों का जंगल ' कहा है , क्योंकि इसमें एक सौ के लगभग छन्दों का प्रयोग है । इसमें से कुछ छन्द ऐसे हैं जिसका न तो पहले प्रयोग हुआ था तथा न ही छन्दशास्त्र में उनका उल्लेख मिलता है । ' पद्मावती समय में पांच प्रकार के छन्द मिलते हैं- दुहा , गाथा , कवित्त , पद्धरी तथा भुजंगी । संक्षिप्त वर्णन के लिए तो कवि दोहा तथा गाथा जैसे छोटे छन्दों का वर्णन करता है , परन्तु विस्तृत वर्णन के लिए कवित्त तथा पद्धरि का प्रयोग करता है । फिर भी दुहा छन्द उनका सर्वाधिक प्रिय छन्द माना गया है ।
भाषा
पृथ्वीराज रासो की भाषा के बारे में लम्बे काल से विवाद चला आ रहा है इसका प्रमुख कारण यह है कि इसमें भाषा के अनेक रूप मिलते हैं । इसमें कहीं तो अपभ्रंश के शब्दों की भरमार है तो कहीं रीतिकाल की भांति ब्रज - भाषा की । इसी भाषा भेद के कारण कुछ लोग रासो को अप्रमाणिक भी सिद्ध करते हैं । पद्मावती समय की भाषा में भले ही कहीं - कहीं अपभंश की भरमार है , लेकिन इसका मूल गठन तो अपभ्रंश ही लगता है । इस भाषा में डिंगल के साथ - साथ पिंगल दोनों भाषा का मिश्रण है । जहां कवि कोमल भावनाओं और रूपों का चित्रण करना चाहता है वहां ब्रजभाषा की कोमल पदावली का सुन्दर रूप उभर आता है । पद्मावती के रूप सौन्दर्य का चित्रण करते समय कवि ब्रज अर्थात् पिंगल का ही सहारा लेता है , यथा
- " मनहुँ कला ससिमान , कला सोलह सो बन्निय ।
- बाल बैस ससि ता समीप अंमित रस पिन्निय ।।
- बिगसि कमल बिग अमर , बैन , पंजन नक लुटिय ।
- हीर कीर अरू बिम्ब मोति नष सिष अहि घुट्टिय ।।
परन्तु युद्ध के वर्णनों में भाषा में ओज गुण की प्रधानता आ जाती हैं ऐसे स्थल पर कवि डिंगल भाषा का प्रयोग करने लगता है । डिंगल भाषा का प्रयोग करते समय कवि ने अरबी , फारसी , तुर्की आदि विदेशी भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग कर दिया है । परन्तु इसे यह मान कर चलना पड़ेगा कि चंदबरदाई की भाषा शैली विषयानुरूप है । वह जिस किसी भाव , विषय या दृश्य का वर्णन करते हैं , उनकी भाषा शैली उसी का बिम्ब प्रस्तुत कर देती है । जैसे-जैसे भाव बदलते हैं , वैसे-वैसे उनकी भाषा अपने स्वरूप को बदल लेती हैं वस्तुतः भाषा पर कविचन्द का आसाधारण अधिकार है । काव्य रचना के आरम्भ में यदि कवि कोमलकांत पदावती का सरस प्रयोग करता है तो आगे चलकर उनकी भाषा अंगारे बरसाने लगती है । विशेषकर वीर , भयानक और रीत रसों का वर्णन करते समय कवि की भाषा ओज गुण प्रधान बन जाती है ।
इस प्रकार हम देखते हैं कि भाव और भाषा दोनों दष्टियों से ' पद्मावती समय एक श्रेष्ठ खण्ड काव्य है । भले ही कवि ने काल्पनिक कथानक की उद्भावना की हो , लेकिन उन्होंने इसे काव्य रचना का रूप देकर पूर्णतः प्रभावशाली बना दिया है । एक विद्वान आलोचक ने उनकी भाषा के बारे में लिखा है- " चन्द बरदाई भाषा के धनी कलाकार हैं । भाषा मानों उनके संकेतों पर नाचती - सी चलती है । भाव और वर्ण्य विषय की पूर्ण सफलता से भाषा भावानुकूल नए - नए रूप धारण करती है उसने बहुत कम शब्दों में बहुत कह डालने निश्चय ही पद्मावती समय भाव - पूर्ण श्रृंगार और वीर रस से समन्वित आकर्षक रचना है । इसकी योजना से पृथ्वीराज रासो को अनूठी गरिमा मिली ।
पृथ्वीराज का चरित्र - चित्रण
पृथ्वीराज चौहान इस कथा का नायक है । सारा कथानक इनके इर्द - गिर्द घूमता है । उसके पिता का नाम सांभर नरेश सोमेश्वर है । कवि ने उसकी आयु केवल 16 वर्ष बताई है । वह दिल्ली का एक वीर और प्रतापी राजा है । शुक उसे पद्मावती के समक्ष इन्द्र का अवतार कहता है । यह कामदेव के समान सुन्दर और रूपवान है । शुक उसका परिचय देता हुआ कहता भी है कि उसके समान्य प्रभावी व्यक्तित्व का कोई है ही नहीं
- " कामदेव अवतार हुआ,सुख सोमेसर नन्द ।
- सास - किरन झलहल कमल , रति समीप वर बिन्द ।। "
आदर्श नायक
कवि ने पृथ्वीराज को महाकाव्योचित नायक सिद्ध करने का प्रयास किया है । यही कारण है कि चन्दबरदवाई ने उसके रूप - सौन्दर्य का अधिक वर्णन नहीं किया , बल्कि वह उसके शौर्य और साहस का अधिक वर्णन करता है । उसकी भुजाएं घुटनों तक लम्बी हैं तथा वह अचूक शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण है । वह बड़ा दानी , शीलवान् साहसी , दृढ प्रतिज्ञ तथा धैर्यवान योद्धा है । उसने गजनी के बादशाह शहाबुद्दीन गौरी को युद्ध में तीन बार हराकर कैद किया और फिर अभयदान देकर छोड़ दिया ।
- " वैसह बरीस घोड़ा नरिन्दं,आजनु बाहु भुअलोक यंयं ।
- जिहि पकरि साह साहाब लीन , तिहुं बेर करिल पानीप हीन ।
- सिंगिनि सुसद्ध गुने चढ़ि जंजीर , युक्के न सबद वेधन्त तीर ।।
- बल बैन करन जिमि दान मानं , सत सहस सील हरिश्चन्द समान ।
- साहस सुकम विक्रम जु वीर , बांनय सुमत अवतार धीर ।।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प थ्वीराज एक सर्वगुण सम्पन्न नायक है । यदि वह कामदेव के समान सुन्दर है तो वह वीर और प्रतापी भी है । नायक के इन्हीं गुणों को सुनकर पद्मावती उस पर आसक्त हो जाती है ।
वीरता की साक्षात् मूर्ति
पृथ्वीराज वीरता का तो साक्षात , अवतार दिखाई देता है । युद्ध क्षेत्र में ही पाठक उसकी वीरता को जान पाता है । वह पद्मावती का हरण कर उसे अपने घोड़े पर बिठाकर दिल्ली की ओर जा रहा था । थोड़ी दूर जाने पर ही शत्रुओं के घुड़सवारों ने उसे चारों ओर से घेर लिया । यह देखकर पृथ्वीराज अपने घोड़े की लगाम मोड़कर पीछे चल पड़ा और उसने अपनी तलवार के वे जौहर दिखाए उसे देखकर मानो सूर्य भी रुक सा गया । धरती कांपने लगी और शेषनाग बेचैन हो उठा । शत्रुओं को पृथ्वीराज काल के समान दिखाई देने लगा । कवि लिखता
- " उल्टी जु राज पथिराज बाग ।
- थकि सूर गगन धर धसत नाग ।।
- सामन्त सूर सब काल रूप ।
- गहि लोह बाहै सुभूप ।। "
उदात्त
इस खण्ड काव्य के अन्तिम भाग में पृथ्वीराज का धीरोदात्त नायक रूप हमारे सामने उभर कर आता है । दिल्ली पहुंच कर वह विधिवत पद्मावती के साथ विवाह करता है और फिर याचकों को दान देकर उन्हें सम्मानित करता है । यही नहीं वह अपने शत्रु शहाबुद्दीन को केवल 1000 घोड़ों का दण्ड देकर मुक्त कर देता है । यह उसकी उदारता का ही परिचायक है । भले ही इतिहासकारों ने पृथ्वीराज की निन्दा की है लेकिन पृथ्वीराज ने प्राचीन भारतीय परम्परा का पालन करते हुए शहाबुद्दीन गौरी को प्राणदान देकर छोड़ दिया । इस सम्बन्ध में कवि लिखता
- " बोलि विप्र सीधे लगन्न , सुभ घरी परठ्यि ।
- हरि बांसह महर बनाय , करि थांवरि गठिय ।।
- जावेद उच्चरहि , होम चौरी जु प्रति वर ।
- पद्मावती दुलहिन अनूप , दुल्लह पथिराज नर ।। "
इस प्रकार पृथ्वीराज एक महान नायक है । जिसमें अपूर्व साहस , सौन्दर्य , दया , उदारता और दूर दष्टि है ।
पद्मावती का चरित्र – चित्रण
पद्मावती ' पद्मावती समय ' की नायिका है । वह समुदशिखर के राजा विजय की पुत्री है । उसकी माता का नाम ' पद्मसेन ' है । ( पद्मावती ) वह 10 राजकुमारों की अकेली बहन है । वह चन्द्रमा की सोलह कलाओं के समान अनिन्द्य सुन्दरी है । उसकी चारित्रिक विशेषताओं का परिचय इस प्रकार
परम सुन्दरी
कविवर चन्दबरदाई ने पद्मावती में पदमिनी नायिका के सभी लक्षणों को घटाने का प्रयास किया है । एकनिष्ठ प्रेमिका होने के साथ - साथ वह अनिंद्य सुन्दरी भी है । वयःसन्धि को प्राप्त उसमें कलाएं हैं । वह 14 विद्याओं और वेदशास्त्र के ज्ञान से परिपूर्ण है । उस युग की अन्य नायिकाओं के समान उसमें वे सभी गुण है जो एक नायिका में होने चाहिए । कवि ने उसे सामुदिक शास्त्र शुभ लक्षणों से युक्त बताया है । काव्य के आरम्भ में ही कवि उसके अनुपम सौन्दर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि
- " मनहं कला ससि भांन कला सोलह सौ बन्निय ।
- बाल बेस ससिता समीप , अंमिन रस पिन्निय ।।
- बिगसि कमल मिग अमर , बैन , पंजन मग लुट्टिय ।
- हीर कीर अरू बिम्म , मोति नप सिनमदबलय अहि घुटिटय ।
- छप्पति गयन्द हरि हंस गति , बिह बनाय संचे सचिय ।
- पद्मिनिय रूप पद्मावतिय , मनहुं काम कामिनि रचिय ।। "
विदूषी नायिका
ऊपर के पद्य में कवि ने पद्मिनी नायिका के सभी गुण गिनवाए हैं । शुक भी उसके अप्रतिम और अनिंद्य रूप देखकर उसे पदमिनी नायिका घोषित करता है । केवल सुन्दर होने से कोई नायिका पद्मिनी ' नायिका नहीं हो सकती । उसमें सामुद्रिक लक्षण होना भी जरूरी है इसलिए कवि ने उसके बारे में लिखा है
- " सामुद्रिक लच्छन सकल , चीसठि कला सुजान ।
- जानि चतुरदस अंग पट , रति बसन्त परमान ।।
कवि उसे पद्मिनी नायिका सिद्ध करने के लिए यह स्पष्ट करता है कि उसके शरीर से कमल की सुगन्ध उत्पन्न होती है । हंस की गति के समान यह मंद - मंद गति से चलती है । भरम्र उस पर मंडराते हैं और उसके शरीर से सुगन्ध फूट - फूट पड़ती है । इसलिए यह एक पद्मगंधा नायिका है ।
- " कमलगंध , वयसंध , हंसगति चलत मंद - मंद ।
- भमर भयहि भुल्लाहिं सुभाव मकपच्च बास रस ।। "
मुग्धा नायिका
अवस्था की दृष्टि से पद्मावती को एक मुग्धा नायिका कहा जा सकता है । वह अभी वयःसन्धि की अवस्था में है । इसका मतलब यह है कि अभी तक उसका बचपन पूरी तरह से गया नहीं । यौवन चोर दरवाजे से उसमें प्रवेश कर रहा है । जब वह तोते को देखती है तो उसे पकड़ कर सोने के पिंजरे में बंद कर देती है और अपना सारा समय उसी के साथ बिताने लगती है । वह अपना खेल - कूद भूलकर तोते को राम - नाम सिखाने में लगी रहती है
- " सपियन संग खेलत फिरत , फिरत , महलनि बाग - निवास ।
- कीर इक्क विनिय नयन , तब मन भयो हुलास ।। "
- तिही महल रणत भवय , गझ्य खेल सब भुल्ल ।
- चित्त चहुंदयौ कीर सौं , राम पढ़ावत फुल्ला । "
विरहिणी नायिका
- अभी तक पद्मावती का रूप एक मुग्धा नायिका का था परन्तु शीघ्र ही वह बाल्यावस्था को छोड़कर यौवनावस्था में प्रवेश करती है । बेटी में यौवन के लक्षण देखकर माता पिता को उसके विवाह की चिन्ता सताने लगती है । वे अपने कुल पुरोहित को भेजकर उसकी सगाई कुमायूं नरेश कुमोदमणि ' से कर देते हैं । लेकिन पद्मावती तो मन से पृथ्वीराज से प्रेम करती थी । वह विरहिणी नायिका के समान अपने मन चाहे वर पृथ्वीराज की बड़ी व्याकुलता से प्रतीक्षा करती है यह विरहिणी का शुद्ध रूप नहीं है । उसके मन में तो एक ही डर है कि कहीं उसका विवाह कुमोदमणि के साथ न हो जाए , क्योंकि कुमोदमणि बारात लेकर समुद्रशिखर आ पहुंचा है । इसलिए वह शुक के साथ पत्र भेजकर पृथ्वीराज को निश्चित तिथि पर आने आग्रह करती है । ऐसा करते समय वह अपनी वंश - मर्यादा , पिता का सम्मान और लोकापवाद की परवाह नहीं करती । पद्मावती का विरहिणी रूप हमारे सामने उस समय उभर कर आता है जब कुमोदमणि के साथ उसकी सगाई हो जाती है और बारात आने का उसे समाचार मिल जाता है । पत्र लेकर शुक दिल्ली चला गया । उधर नगर बाहर बारात पहुंच चुकी थी । उधर पद्मावती दुःख में डुबी हुई शुक के लौटने की प्रतीक्षा करने लगी । मैले कपड़े पहने रोती हुई झरोखे में बैठी वह एक टक दृष्टि बांधे दिल्ली की ओर से आने वाले मार्ग को देख रही थी । कवि उसकी विरह व्यथा का वर्णन करते हुए लिखता है
- " विलपि अवास कुंवर बरन , मनो राहु छाया सुरत ।
- संपति गयमि पलकि , विथित पंथ दिल्ली सपति ।। "
पदमावती दिल्ली की ओर से आने वाले मार्ग पर लगातार आखें गड़ाए देख रही थी । जब वह शुक उसे आकर मिला तो वह प्रफुल्लित हो उठी । शुक के मुख से पृथ्वीराज का संदेश सुनकर उसके नेत्र आनन्द से भर गए ।
आदर्श प्रेमिका
पद्मावती एक क्षत्रिय की बेटी है । पृथ्वीराज के प्रति उसका प्रेम एकनिष्ठ है । संकट की घड़ी में वह बुद्धि और साहस दोनों का प्रयोग करती है । जब वह देखती है कि कुमोदमणि से उसका विवाह होने जा रहा है तो वह शुक को पत्र देकर उसे तत्काल दिल्ली भेज देती है । यहीं नहीं वह पत्र में यह भी लिख देती है कि किस तिथि को उसका विवाह हो रहा हैं वह पृथ्वीराज को आग्रह करती है कि उसी तिथि को वह मंदिर में आकर उसका हरण कर ले । यह सारी योजना वह स्वयं बनाती है । इससे पता चलता है कि यह एक साहसी है और पृथ्वीराज के प्रति उसका एकनिष्ठ प्रेम है । जब शुक उसे पृथ्वीराज के आने का समाचार सुनाता है तो वह आनन्दित हो उठती है । तब वह अपनी विरहावस्था भूल जाती है । तब वह मैले वस्त्र उतारकर स्नान करती है और आभूषणों से सोलह श्रृंगार करती ।
- " तन चिकट चीर डायो उतारि ।
- मज्जन मयंक नवसत सिंगार ।।
- भूषन मंगाय नव सिनमदबलप अनुष ।
- सजि सेन मनो मनमण्य भूप ।। "
वह सज - धज कर सखियों के साथ मंदिर में पूजा करने जाती है । पूजा के बाद वहां पृथ्वीराज को देखकर उसकी तरफ मंद - मंद मुस्कान से देखती हुई हल्का सा घूंघट कर लेती है । इस प्रकार वह जहां एक और पृथ्वीराज के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करती है वहीं दूसरी और उसे प्रेरित करती है कि वह उसका हरण कर ले ।
इस प्रकार हम देखते हैं कि पद्मावती एक महाकाव्योचित्त नायिका है । उसमें पद्मिनी नायिका के सभी गुण विद्यमान हैं । वह केवल अनुपम सुन्दरी ही नहीं , विदुषी भी है । एक क्षत्रिय कन्या होने के कारण संकट की घड़ी में वह असहाय होकर रोती नहीं , बल्कि बुद्धि और साहस का परिचय देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है । निश्चय ही पद्मावती एक वीरांगना युवती है ।
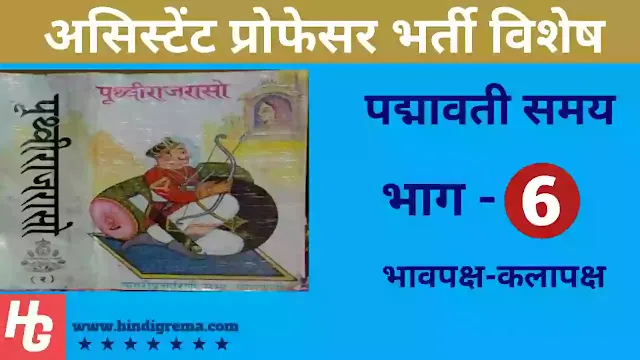
1 comments:
Click here for commentsNice
उत्साहवर्धन के लिये धन्यवाद!
आपकी टिप्पणी हमें ओर बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है । ConversionConversion EmoticonEmoticon